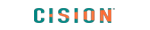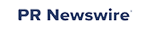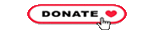-श्रीराम माहेश्वरी, भोपाल
भारतीय संस्कृति और वेदों में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का हमें उल्लेख मिलता है। हमारे यहां आदिकाल से ही पेड़ों की पूजा करने का रिवाज रहा है । भारत में औषधीय पौधों का रोपण और संरक्षण किया जाता रहा है। वनस्पति शास्त्र का महत्व रहा, इसीलिए आयुर्वेद का प्रचलन भी निरंतर बढ़ा है। महामारी के इस संकट के समय में आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से नागरिकों को अच्छा लाभ हुआ है। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेदिक औषधियां रामबाण साबित हुई हैं। प्रकृति में औषधीय पौधों का महत्व हमें समझना होगा। तभी हम आयुर्वेद को बढ़ावा देने में समर्थ हो सकेंगे। सही मायने में इन पौधों और वनस्पतियोंको बढ़ावा देने से ही पर्यावरण का संरक्षण होगा।
भारत में पिछले चार दशकों में उद्योगों को खूब बढ़ावा दिया गया। उद्योग धंधे भी बढ़े, परंतु औद्योगिक क्रांति के इस विकास के साथ-साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता रहा। उद्योगों से निकलने वाला विषैला तरल पदार्थ और अपशिष्ट नदियों और जलाशयों में मिलने लगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पेयजल स्रोत दूषित होते गए। भूमि में काफी नीचे तक इस हानिकारक पदार्थों ने नुकसान पहुंचाया। इससे कुएं, बावड़ी और हैंडपंप जैसे जल स्रोतों से हमें प्रदूषित जल मिलने लगा और दूषित जल के सेवन से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ा। कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। भूमि की उर्वरा शक्ति रासायनिक खाद के उपयोग से नष्ट होती चली गई। फसल कटाई के बाद किसान हर साल खेतों में नरवाई जलाते हैं। इससे भूमि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पक्षियों का भी भोजन नष्ट हो जाता है। इस तरह की समस्याओं का हमें समाधान खोजने की आवश्यकता है।
विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल पांच जून को मनाते हैं। इस दिन दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। करीब एक सप्ताह तक तो लोगों में उत्साह बना रहता है और फिर स्थिति पूर्ववत हो जाती है। यदि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आने वाला समय हरित क्रांति का होगा। आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता रहेगा।
वेदों और शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर हम अपने परिवेश को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। महानगर शहरों का अधिग्रहण कर रहे हैं और शहर और कस्बे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण परिवेश पर शहरी संस्कृति हावी होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है। बहुमंजिला इमारतें, सड़कें, पुलों का निर्माण, उद्योगों का विस्तार होने से कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है। पड़त और चरनोई की भूमि नष्ट होने से पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है। इससे पशुओं की संख्या भी कम हो रही है।
वनों के घटने और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से वन्य प्राणियों के जीवन पर भी संकट खड़ा हो रहा है। वे जंगल छोड़कर अब गांव और शहरों में आने लगे हैं। जंगलों में मानवीय गतिविधियां बढ़ने से और शोर बढ़ने से पशु पक्षियों को रहन-सहन और प्रजनन की समस्या बढ़ी है। जिससे उनके जीवन पर भी संकट बढ़ रहा है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का असर शहरों के साथ-साथ गांव में भी देखने को मिल रहा है। खेतों में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिजली के लिए हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना होगा।
सार्वजनिक परिवहन के लिए हमें बड़ी डीजल बसों की बजाय छोटे बैटरी के वाहन उपयोग में लाने होंगे। इससे प्रदूषण नहीं होगा। डीजल कारों की बजाय पेट्रोल कारों के चलन की अनुमति होना चाहिए। इससे कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण हो सकेगा। एसी और फ्रिज के बढ़ते प्रचलन को भी हमें हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।
शहरों में कचरे के निस्तारण की समस्या विकराल रूप ले रही है। सड़कों और रेल पटरी के किनारे, गलियों और मोहल्लों में कचरे के ढेर नजर आ जाते हैं। नागरिकों को स्वच्छता की ओर ध्यान देना होगा। उन्हें नगर निगम और नगर पालिका के बजाय स्वयं की भी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्वच्छता अभियान का हर नागरिक को हिस्सा बनना होगा, तभी हम कचरे का समाधान कर पाएंगे।
किसी देश की जैव विविधता जितनी समृद्ध होगी, वह देश भी उतना ही अधिक खुशहाल होगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों और वनस्पतियों का संरक्षण करना होगा। हर नागरिक अपने घर के आस-पास कम से कम दो पेड़ लगाए। उनका संरक्षण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें। ध्वनि, वायु, भूमि और जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में वे अपना योगदान दें तभी हम सही मायने में पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे।
(लेखक 'नेचर इंडिया' के संपादक एवं 'पर्यावरण और जैव विविधता' पुस्तक के लेखक हैं )