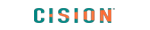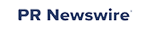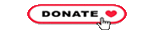उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब के लिये लगातार कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराने और उस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लग रहे आरोपों के बीच एक संसदीय समिति ने देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक साल से अधिक समय का निर्धारित करने की सिफारिश की है।
समिति की इस सिफारिश पर यह सवाल उठना स्वाभाविक होगा कि आखिर देश की स्वतंत्र न्यायपालिका के इतिहास में अभी तक कभी ऐसा महसूस क्यों नहीं किया गया और अब इस तरह का सुझाव संसदीय समिति ने क्यों दिया ?
संसदीय समिति ने प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तय कार्यकाल नहीं होने की वजह से न्यायिक सुधारों में आ रही दिक्कतों पर विस्तार से गौर करने के बाद इस बारे में सुझाव दिया है।
समिति ने न्यायिक सुधारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के बाद यह महसूस किया कि प्रधान न्यायाधीश का तय कार्यकाल होना चाहिए ताकि वह न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णय ले सकें क्योंकि वह कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं के संदर्भ में संसदीय समिति ने कहा है, 'यदि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी ढांचा है तो संसदीय लोकतंत्र संविधान का ज्यादा बड़ा बुनियादी ढांचा है और न्यायपालिका संसद के अधिकारों को छीन नहीं सकती है।'
कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या, उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जैसे अनेक बिन्दुओं पर विचार किया है।
संसदीय समिति ने हालांकि अपनी रिपोर्ट में प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिये कोई न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने की सिफारिश नहीं की है लेकिन ऐसा लगता है कि वह चाहती है कि इस पद पर आसीन न्यायाधीश को अपना कार्य करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
देश के प्रधान न्यायाधीशों के कार्यकाल पर नजर डालने पर पता चलता है कि पिछले 40 सालों में इस पद पर सबसे लंबे समय (सात साल से भी अधिक) तक न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक न्यायमूर्ति के एन सिंह रहे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश रहे जबकि न्यायमूर्ति सिंह 25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर, 1991 तक इस पद पर आसीन रहे।
हालांकि संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'पिछले 20 सालों में उच्चतम न्यायालय में 17 प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किये गये और इनमें से केवल तीन का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक था। इनमें से कई न्यायाधीशों का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम था। भारत के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश (न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू) का कार्यकाल एक माह से भी कम का था।'
इन बीस सालों में एक साल से कम अवधि तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहने वालों में न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी, न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा, न्यायमूर्ति बी. एन. किरपाल, न्यायमूर्ति अलतमश कबीर, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा जैसे न्यायाधीश शामिल हैं। इसी तरह, एक साल से अधिक परंतु दो साल से कम समय तक इस पर रहने वालों में वर्तमान प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर के अलावा न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू (अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष) , न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, न्यायमूर्ति आर. सी .लाहौटी और न्यायमूर्ति वी. एन. खरे शामिल हैं।
इन बीस वर्षों के दौरान दो साल से अधिक के कार्यकाल वाले प्रधान न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी, न्यायमूर्ति डॉ. आदर्श सेन आनंद और न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन शामिल हैं जो क्रमशः 25 अक्तूबर, 1994 से 24 मार्च 1997 तक, 10 अक्तूबर 1998 से 31 अक्तूबर 2001 तक और 14 जनवरी 2007 से 12 मई, 2010 तक प्रधान न्यायाधीश रहे। इनके अलावा, न्यायमूर्ति एस. एच. कपाडिया का प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल भी दो साल से अधिक(12 मई, 2010 से 28 सितंबर, 2012) था।
इसके विपरीत, इस अवधि में प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू का कार्यकाल एक महीने से भी कम यानी दो मई 2004 से 31 मई 2004 तक ही था।
न्यायमूर्ति राजेन्द्र बाबू से पहले 1991 में देश के प्रधान न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति के. एन. सिंह का कार्यकाल सिर्फ 17 दिन और न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक का कार्यकाल सिर्फ 40 दिन का ही था। न्यायमूर्ति के. एन. सिंह 25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक और न्यायमूर्ति पटनायक 8 नवंबर, 2002 से 18 दिसंबर, 2002 तक इस पद पर थे।
समिति का यह विचार पूर्णतया तर्कसंगत है कि प्रधान न्यायाधीश का अल्प कार्यकाल होने की वजह से उन्हें कोई बड़ा सुधार (न्यायिक) या दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता है। समिति की इस सिफारिश पर अब सरकार को ही विचार करके निर्णय लेना है।
समिति का मानना है, 'प्रधान न्यायाधीश को बार -बार बदले जाने की वजह से कोई भी महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार, जिनके लिये उनका लंबे समय तक बना रहना आवश्यक होता है, संभव प्रतीत नहीं होता है।'
समिति का मत है कि संसद को न्यायपालिका में नियुक्ति हेतु प्रक्रियागत कानून लाना चाहिए क्योंकि प्रक्रियागत कानून के अभाव ने न्यायपालिका को कार्यकारी कृत्य में हस्तक्षेप के लिये जगह प्रदान कर दी है। इसी तरह, समिति चाहती है कि उच्च न्यायालयों में(न्यायाधीशों के) स्थानांतरण और तैनाती प्रणाली को भी संविधान में संशोधन कर प्रवर्तित किया जाये।
उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून और इससे संबंधित संविधान संशोधन पहले ही निरस्त कर चुकी है। इसके बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्तियों और न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में समिति की राय है कि संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया और इसके मापदंड को सहज बनाया जा सके। समिति का स्पष्ट मत है, 'न्यायपालिका में बढ़ी संख्या में रिक्तियों के लिये नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली जिम्मेदार है।'
उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को लेकर बार- बार उठाये जा रहे सवालों पर यही जवाब पर्याप्त लगता है कि 25 साल में पहली बार उच्च न्यायालयों के लिये एक साल (2016) में सर्वाधिक 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी जो एक रिकार्ड है। देश के 24 उच्च न्यायालयों के लिये न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 1079 है और अभी भी इनमें चार सौ से अधिक पद रिक्त हैं।
उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन में भाई- भतीजावाद के आरोप समय- समय पर लगते रहे हैं। समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे दोहराते हुये कहा है, "हमारे पास ऐसे उदाहरण विद्यमान है जहां तीन पीढि़यों से लोगों की नियुक्ति न्यायपालिका में हो रही है। जिला और उच्च न्यायालय में ऐसे मेधावी लोग हैं जिन्हें न्यायपालिका में पहुंचने का कभी अवसर नहीं मिलता है।'
चूंकि संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने के अपने फैसले में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का जिक्र करते हुये इसके प्रक्रिया ज्ञापन में सुधार पर जोर दिया था, इसलिए लंबे समय से अपेक्षा की जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रक्रिया ज्ञापन, जो अगस्त महीने से प्रधान न्यायाधीश के समक्ष है, को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जायेगा।
उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया से संबंधित इस प्रक्रिया ज्ञापन को सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिये जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिल सकती है।
- अनूप कुमार भटनागर
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं